एक साधारण-सा वाक्य और पूरा सोशल मीडिया मानो अलार्म मोड में चला गया।
टाइमलाइन पर अचानक नैतिकता के प्रवचन शुरू हो गए।
कोई इसे घमंड बता रहा है, कोई जातिवाद, तो कोई समाज को पीछे ले जाने वाली सोच।
लेकिन सवाल यह है—
क्या समस्या उस वाक्य में है, या उस सिस्टम में जिसने जाति को हर जगह ज़रूरी बना रखा है?
जाति का इस्तेमाल जब सिस्टम करे, तो जायज़?
हम उसी समाज में रहते हैं जहाँ:
- सरकारी फॉर्म बिना जाति के पूरे नहीं होते
- एडमिशन, नौकरी और स्कॉलरशिप जाति के आधार पर तय होती हैं
- चुनावों में वोट खुलेआम जाति देखकर मांगे जाते हैं
- शादी के विज्ञापनों में जाति पहली पहचान बनती है
- अस्पताल से लेकर राशन कार्ड तक, हर जगह जाति पूछी जाती है
यानी जाति यहाँ कोई छुपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि एक संस्थागत पहचान है।
राजनीति में जाति ताकत है, लेकिन ज़ुबान पर अपराध?
नेता अपनी गाड़ियों पर जाति लिखवाते हैं।
इलाकों के बाहर बोर्ड लगते हैं।
राजनीतिक पहचान जाति से बनती और बिगड़ती है।
लेकिन जब वही पहचान कोई आम व्यक्ति—खासतौर पर एक लड़की—अपने बचाव में बोल दे,
तो वही समाज अचानक असहज हो जाता है।
यह विरोधाभास नहीं तो और क्या है?
पहचान सिस्टम देता है, दोष इंसान को?
कोई बच्चा जन्म से अपनी जाति नहीं चुनता।
स्कूल, समाज और व्यवस्था उसे बार-बार बताती है—
“तुम यह हो।”
जब सालों तक वही पहचान थोपी जाए
और एक दिन वही व्यक्ति उसे शब्दों में कह दे,
तो इसे अपराध कहना कहां का न्याय है?
असली सवाल: जाति बोलना या जाति चलाना?
अगर जाति:
- नीति बनाने में सही है
- लाभ देने में जरूरी है
- नुकसान पहुँचाने में मान्य है
- राजनीति में हथियार है
तो फिर उसे ज़ुबान पर लाना गलत कैसे हो गया?
समस्या जाति के अस्तित्व से नहीं,
समस्या हमारी चयनात्मक नैतिकता से है।
दोगलापन यही है
जब सिस्टम जाति बनाए, बाँटे और उससे फ़ायदा उठाए—
तो सब सामान्य।
लेकिन कोई इंसान उसी पहचान को स्वीकार कर ले—
तो बवाल।
शायद हमें उंगली उठाने से पहले
आईने में खुद से एक सवाल पूछना चाहिए:
क्या हमने कभी अपनी जाति से फायदा नहीं उठाया?
क्या हमने कभी भीतर ही भीतर उस पहचान पर गर्व नहीं किया?
अगर जवाब “हाँ” है,
तो फिर गुस्सा किसी और पर नहीं,
अपने दोहरे मापदंडों पर होना चाहिए।




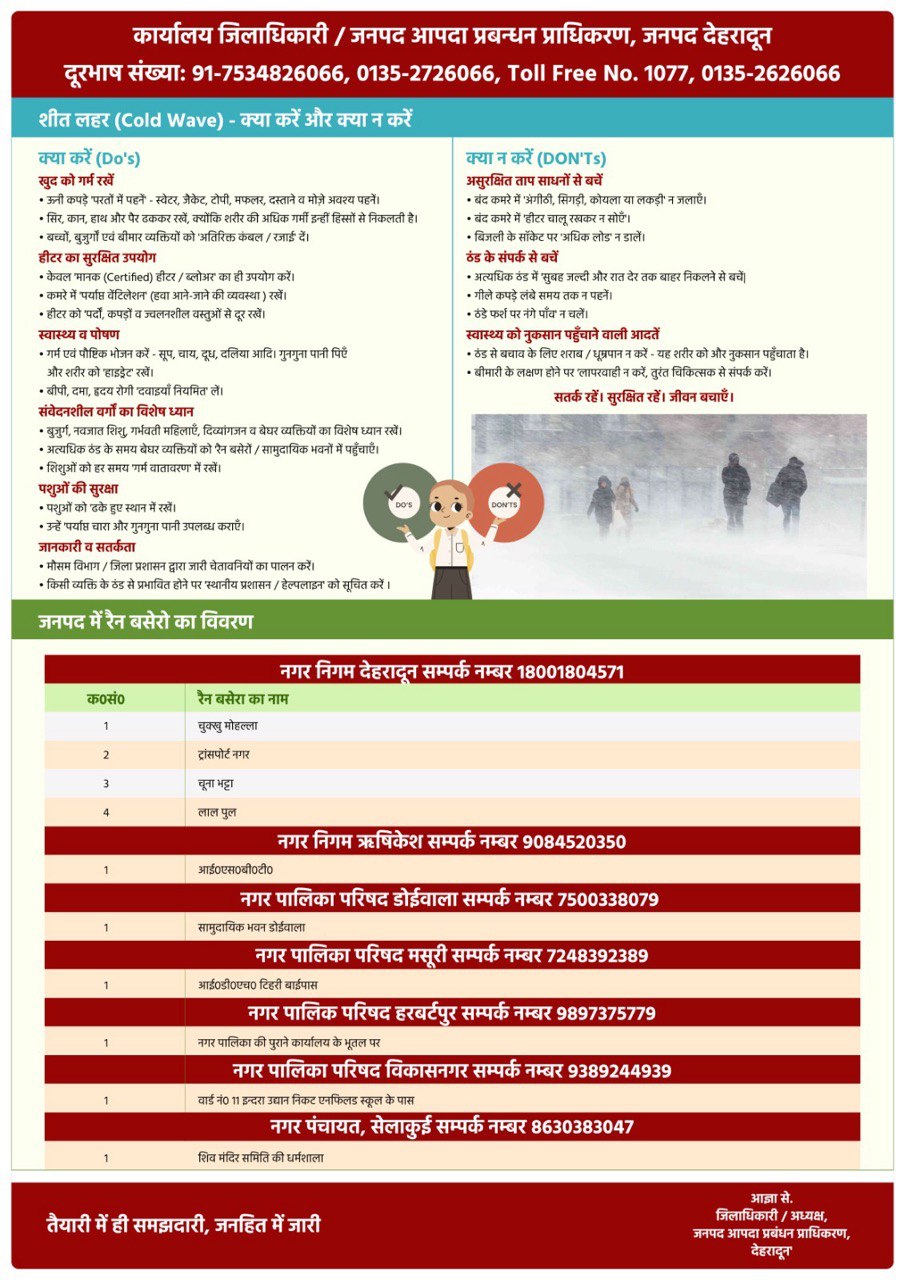









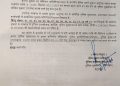


Discussion about this post